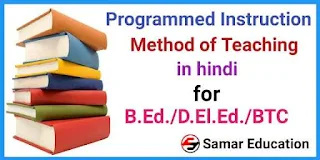 Programmed Instruction Method of Teaching in hindi" width="576" height="288" />
Programmed Instruction Method of Teaching in hindi" width="576" height="288" />अभिक्रमित अनुदेशन वह अध्ययन है जिसमें पाठ्यसामग्री को छोटे-छोटे पदों में विभाजित करके शृंखलाबद्ध किया जाता है तथा इसे छात्रों के समक्ष क्रमानुसार प्रस्तुत करके कम गलतियाँ करते हुए उन्हें नवीन एवं जटिल विषय-वस्तु की शिक्षा उनको गति के अनुसार प्रदान की जाती है। इस सारो प्रक्रिया में छात्रों को अपनी प्रगति के ज्ञान के द्वारा पृष्ठ-पोषण दिया जाता है।
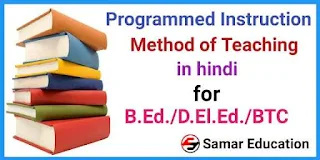 Programmed Instruction Method of Teaching in hindi" width="576" height="288" />
Programmed Instruction Method of Teaching in hindi" width="576" height="288" />
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:- अभिक्रमित अनुदेशन के बीच पञ्चतन्त्र की कहानियों और गीता में देखने को मिलते हैं। प्रारम्भिक व्यवहार, अन्तिम व्यवहार, छोटे-छोटे पद, कार्य की प्रगति को तुरन्त ज्ञान एवं मूल्यांकन आदि सभी अनुदेशन के पद गीता में प्राप्त होते हैं किन्तु पाश्चात्य विद्वान मानते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन का विचार 2000 वर्ष पूर्व यूनानी दार्शनिक सुकरात ने दिया। सुकरात प्रश्नोत्तर विधि से अध्यापन करवाते थे। प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाने पर छात्रों को प्रत्यय स्पष्ट हो जाता था। यह भी स्वीकार किया जाता है कि सुकरात द्वारा बनाए गए रेखागणित पर संवाद के रूप में अभिक्रमित अनुदेशन की प्लेटों ने लिपिबद्ध किया जो सुकरात के शिष्य थे।
सन् 1912 में ई. एल. थार्नडाइक ने अभिक्रमित अनुदेशन में साम्यता रखने वाली शिक्षण विधि की कल्पना की। सन् 1920 में सिडनी एल. प्रैसी ने एक ऐसी शिक्षण मशीन का निर्माण किया जिसके द्वारा छात्रों के समक्ष प्रश्नों की एक श्रृंखला उपस्थित हो जाती थी और छात्रों को प्रश्नों का उत्तर देने के एकदम बाद ही अपने उत्तर के सही या गलत होने की जानकारी मिल जातो थो। छात्र इससे अपनी प्रगति का ज्ञान प्राप्त करते हुए अपने निर्धारित उद्देश्यों की ओर जाने के लिए दुगुनी शक्ति से प्रेरित होकर तैयारी में लग जाते थे।
इसके पश्चात् हरबर्ट विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बी.एफ. स्कीनर ने सोखने पर अनेक प्रयोग किए तथा जैम्स जी. हालैण्ड के सहयोग से स्व-शिक्षण सामग्री का निर्माण किया, जिसे आज अभिक्रमित अनुदेशन अथवा अभिक्रमित अधिगम का आधार माना जाता है। स्कीनर ने शिक्षण अधिगम का एक मॉडल तैयार किया। यह अभिक्रमित हो आज रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन कहलाता है।
1. स्मिथ व पूरे के शब्दों में, "अभिक्रमित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक क्रिया है, जिसके द्वारा छात्रों को उनकी परिचित पृष्ठभूमि से एक नवीन तथा जटिल तथ्यों, सिद्धान्तों तथा अवबोधों की ओर ले जाया जाता है।"
2. डी.एल. कुक के शब्दों में, "अभिक्रमित अधिगम, स्व- शिक्षण विधियों के व्यापक सम्प्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त एक विद्या है।"
3. स्टोफल के शब्दों में, "ज्ञान के छोटे अंशों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने का अभिक्रमित तथा इसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया की अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं।"
उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि अभिक्रमित अध्ययन वह अनुदेशन है जिसमें पाठ्य सामग्री को छोटे पदों में विभाजित करके शृंखलाबद्ध किया जाता है तथा इसे छात्रों के समक्ष क्रमानुसार प्रस्तुत करके, कम से कम गलतियां करते हुए सीखने का अवसर देता है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती। इसमें व्यक्तिगत अनुदेशन के रूप में सीखने के लिये अवसर दिया जाता है। इसमें छात्र तत्पर होकर अपनी गति के अनुसार सीखता है और ज्ञान प्राप्ति का भी बोध करता है। इसे व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया मानते हैं।
शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए योजना का निर्माण करते समय कुछ सिद्धान्तों की अनुपालना की जाती है। वास्तव में ये व्यावहारिक सिद्धान्त हैं। ये सिद्धान्त अभिक्रमित अधिगम की व्यवस्था करते हैं। इन सिद्धान्तों का प्रतिपादन मनोविज्ञान की प्रयोगशाला के शोध कार्यों के आधार पर किया गया है। इन सिद्धान्तों में से प्रमुख निम्न प्रकार से है-
1. छोटे-छोटे पदों का सिद्धान्त:- शिक्षार्थी को अधिगम कराते समय अभिक्रमित सामग्री में पाठ्य-वस्तु को छोटे-छोटे पदों में व्यवस्थित कर छात्रों के समक्ष एक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक पद में छात्रों को अनुक्रिया करने के लिए रिक्त स्थान दिया जाता है। पद को अनुक्रिया उसके साथ ही दी जाती है। छात्र उस पद का अध्ययन करते समय सही उत्तर को छिपाकर रखता है तथा एक समय में एक पद का ही अध्ययन करता है। इस सिद्धान्त के आधार पर अध्ययन करने से छात्र विषय-वस्तु को सरलता से सीखता है तथा पाठ्य वस्तु को आत्मसात् कर लेता है।
2. व्यवहार विश्लेषण का सिद्धान्त:– अभिक्रमित अनुदेशन में शिक्षण सामग्री को छोटे-छोटे पदों में विभाजित करते समय सैद्धान्तिकता के स्थान पर व्यवहारिकता को बल दिया जाता है ताकि छात्र पद के प्रति व्यवहार करके उस पद अथवा शिक्षण सामग्री के ज्ञान को स्थायी बना सकें।
3. सक्रिय सहभागिता का सिद्धान्त:- मनोविज्ञान की प्रयोगशाला के शोध कार्यों को दूसरी उपलब्धि यह है कि छात्र अधिगम के समय यदि सक्रिय रहता है तब वह अधिक सीखता है। अभिक्रमित अनुदेशन के पदों को पढ़ने के बाद छात्र को रिक्त स्थान पूर्ति के लिए समुचित अनुक्रिया करनी होती है। अधिगम का यह सिद्धान्त है कि शिक्षार्थी 'कार्य द्वारा' अधिक सीखता है। अनुदेशन के इस अधिनियम में इस धारणा का अनुसरण किया जाता है। छात्र पदों को सही अनुक्रिया करने के लिए सक्रियता की आवश्यकता होती है।
4. तत्काल पृष्ठपोषण का सिद्धान्त:- पुनर्बलन सिद्धान्त को यह धारणा है कि छात्रों की अनुक्रियाओं की पुष्टि करने से छात्र अधिक सीखता है। पढ़ते समय छात्र तत्पर रहकर जो अनुक्रियाएँ करता है उनकी तत्काल जाँच की जाती है तथा सही अनुक्रिया के लिए सकारात्मक पुनर्बलन मिलने से छात्र अधिक गति से सीखता है।
5. तार्किक क्रम का सिद्धान्त:- अभिक्रमित अनुदेशन में पदों को इस प्रकार तार्किक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है कि पूर्व पद में अग्रिम पद का संकेत प्राप्त हो जाता है, जिससे छात्र में उस पद को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वह अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए क्रमबद्ध रूप से एक के बाद एक पद का अधिगम करता जाता है जिससे छात्र उस विषय वस्तु का पूर्ण जान प्राप्त करने में सफल होता है।
6. स्वगति का सिद्धान्त:– शिक्षार्थी को स्वगति से सीखने का अवसर दिया जाता है तो वह अधिक सोखता है। इस सिद्धान्त का सम्बन्ध व्यक्तिगत भिन्नता से होता है। छात्र पद को पढ़कर अनुक्रिया करता है फिर स्वयं उनकी जाँच करता है, इसके बाद अगले पद को पढ़ता है। इन सभी क्रियाओं में छात्र को स्वतन्त्रता होती है कि वह अपनी क्षमता तथा गति के अनुसार अध्ययन करे। इससे द्रुत गति से पढ़ने वाले छात्रों के समय में चचत होती है तो मन्द गति से पढ़ने वाला छात्र पद को समझकर आगे बढ़ता है। समय घटक के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता को नियन्त्रित किया जाता है।
7. सामग्री वैधता का सिद्धान्त:- शिक्षण उद्देश्यों के अनुसार ही अभिक्रमित अनुदेशन के फ्रेम तैयार किये जाते हैं ताकि उनकी सरलता से प्राप्ति हो सके।
8. छात्र परीक्षण तथा प्रगति ज्ञान का सिद्धान्त:- छात्र को एक फ्रेम का अध्ययन करने के पश्चात् अगले तक जाने के लिए पूर्व पद की प्रतिपुष्टि करनी होती है और ये पद सरल में जटिल नियम पर आधारित होते हैं। छात्र जितने पदों को हल कर लेता है उसके आधार पर उसे अपने ज्ञान की प्रगति का पता चलता रहता है।
शिक्षण प्रक्रिया में अपनाए जाने से होने वाले लाभ निम्न प्रकार हैं-
अभिक्रमित अनुदेशन का शिक्षण में प्रयोग लाभदायी होने पर भी इसकी कुछ सीमाएँ हैं जो निम्न प्रकार हैं-
वर्तमान युग में अभिक्रमित अनुदेशन की उपयोगिता सर्वविदित है। इसका प्रयोग शिक्षा में ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी उपयोग किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग निम्न क्षेत्रों में किया जाता है-
वर्तमान युग में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला अभिक्रमित अनुदेशन अत्यन्त उपयोगी तकनीक के रूप में शिक्षक के हाथ में है, जिसका उपयोग करके शिक्षक अपने छात्रों को गहन जान दे सकता है। इसके माध्यम से विषय वस्तु में पूर्ण निपुणता प्राप्त की जा सकती है।